सारांश (Summary)
Global Warming in Hindi -इस लेख में हमने ये बताया है की ग्लोबल वार्मिंग आज के दौर की एक गंभीर समस्या है, जो पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि का कारण बन रही है। इस लेख में हमने ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारणों, जैसे ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन, वनों की कटाई, और औद्योगिक गतिविधियों पर चर्चा की है। इसके अलावा, इसके प्रभाव, जैसे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, और जैव विविधता के ह्रास का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही, समस्या के समाधान के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, वृक्षारोपण, और वैश्विक स्तर पर सहयोग जैसे उपायों को सुझाया गया है। यह लेख इस महत्वपूर्ण मुद्दे को समझने और इसे नियंत्रित करने की दिशा में एक कदम है। विस्तार के उल्लेख को पड़े.

ग्लोबल वार्मिंग: कारण और समाधान
ग्लोबल वार्मिंग एक गंभीर वैश्विक समस्या है, जो पृथ्वी के तापमान में हो रही स्थिर वृद्धि को दर्शाती है। जो मुख्य रूप से मानव गतिविधियों के परिणामस्वरूप होती है। यह मुख्य रूप से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होती है, जिससे पृथ्वी की सतह गर्म होती जा रही है। इसे जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण भी माना जाता है।, जिनमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), मीथेन (CH₄), और नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) शामिल हैं। इन गैसों का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधनों (कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस) का जलना, औद्योगिकीकरण, कृषि गतिविधियाँ, और वनों की कटाई है। इन गैसों के बढ़ने से सूरज की गर्मी पृथ्वी के वातावरण में फंस जाती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। इसे ग्रीनहाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है।
ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया– Global Warming in Hindi
जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो उनमें से कुछ ऊर्जा पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित की जाती है, और फिर वह ऊर्जा अवरक्त विकिरण (infrared radiation) के रूप में वापस अंतरिक्ष में जाती है। लेकिन, ग्रीनहाउस गैसें इस विकिरण को फँसा लेती हैं, जिससे पृथ्वी के वातावरण में गर्मी फंस जाती है और तापमान बढ़ने लगता है। इसे ग्रीनहाउस प्रभाव कहा जाता है, और यह प्रभाव आवश्यक मात्रा में प्राकृतिक रूप से होना भी आवश्यक है, ताकि पृथ्वी पर जीवन संभव हो सके। लेकिन, मानव गतिविधियों ने इस प्रभाव को बढ़ा दिया है, जिससे असंतुलन हो गया है और तापमान तेजी से बढ़ने लगा है।
ग्लोबल वार्मिंग के कारण
ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारणों में ग्रीनहाउस गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), मीथेन (CH₄), और नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) का उत्सर्जन प्रमुख है। यह गैसें सूर्य की किरणों को अवशोषित करके वातावरण को गर्म करती हैं। इनके बढ़ते स्तर का मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
1.ईंधन का अत्यधिक उपयोग: जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोल और डीजल का व्यापक उपयोग औद्योगिक विकास के साथ-साथ परिवहन और ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। यह CO₂ उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है।
2.वनों की कटाई: पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, लेकिन वनों की कटाई के कारण यह प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे वातावरण में CO₂ की मात्रा बढ़ती है।
3.औद्योगिक गतिविधियाँ: उद्योगों में कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों का जलना बड़े पैमाने पर होता है, जिससे वातावरण में CO₂ और अन्य ग्रीनहाउस गैसें छोड़ी जाती हैं.
4.कृषि और पशुपालन: पशुधन, विशेष रूप से मवेशी, मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है।
5.निर्माण और शहरीकरण: बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है, जिसमें जंगलों को काटकर आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। इससे न केवल वनों की कमी हो रही है, बल्कि ऊर्जा की खपत भी बढ़ रही है।
6.उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग: आधुनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है, जिससे नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन होता है जो वातावरण को गर्म करने में सहायक होती हैं।
7.ऊर्जा और बिजली उत्पादन: ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दुनिया भर में कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता बनी हुई है। पारंपरिक बिजली संयंत्र ग्रीनहाउस गैसों का प्रमुख स्रोत हैं।

ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव – Global Warming in Hindi
ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखे जा सकते हैं:
1.ग्लेशियरों का पिघलना: हिमालय, आर्कटिक और अन्य क्षेत्रों के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र स्तर बढ़ रहा है।
2.प्राकृतिक आपदाएँ: जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखा, और चक्रवात जैसी आपदाएँ बार-बार हो रही हैं।
3.जैव विविधता पर प्रभाव: कई प्रजातियाँ अपने प्राकृतिक आवास के बदलने के कारण विलुप्ति के कगार पर हैं।
4.मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव: बढ़ते तापमान के कारण कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, जैसे हीट स्ट्रोक, अस्थमा, और जलवायु से संबंधित बीमारियाँ। साथ ही, ग्लोबल वार्मिंग से खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ रहा है, जिससे कुपोषण का खतरा बढ़ गया है।
5.जलवायु परिवर्तन: ग्लोबल वार्मिंग जलवायु में बड़े पैमाने पर परिवर्तन कर रही है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में असामान्य मौसम स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं। कुछ जगहों पर सूखा बढ़ रहा है, जबकि कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की घटनाएँ हो रही हैं।
6.पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव: समुद्री जीवन, जलीय और स्थलीय जीव-जंतु ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित हो रहे हैं। समुद्र का तापमान बढ़ने से प्रवाल भित्तियाँ (कोरल रीफ्स) नष्ट हो रही हैं और समुद्री प्रजातियों की संख्या घट रही है।
7. समुद्र स्तर में वृद्धि: ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इसका परिणाम यह है कि तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है।
ग्लोबल वार्मिंग के समाधान
ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कदम उठाना आवश्यक है:
1.नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग: सौर, पवन और जल विद्युत जैसी स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। इससे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी और CO₂ उत्सर्जन घटेगा।
2.वन संरक्षण और वृक्षारोपण: अधिक से अधिक पेड़ लगाकर और वनों की सुरक्षा करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं।
3.ऊर्जा दक्षता: ऊर्जा की बचत और कुशल उपकरणों का उपयोग करने से उत्सर्जन कम किया जा सकता है।
4.स्वच्छ परिवहन: इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए, ताकि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाया जा सके।
5.वैश्विक सहयोग: देशों को पेरिस समझौते जैसे अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौतों का पालन करना चाहिए और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए एकजुट होना चाहिए।
6.जन जागरूकता: लोगों में ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। उन्हें इसके प्रभावों और निवारण के उपायों के बारे में जानकारी देनी चाहिए, ताकि वे अपने दैनिक जीवन में छोटे-छोटे कदम उठाकर इसमें योगदान कर सकें।
- Also Read :
- G20 Summit Full Article – Click Here
- One Nation One Election Hindi Article – Click Here
कुछ अन्य सन्दर्भ – Global Warming in Hindi
1. ग्लोबल वार्मिंग के ऐतिहासिक संदर्भ
औद्योगिक क्रांति (18वीं शताब्दी के अंत से) के बाद ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन तेजी से बढ़ा।
पहले और अब के तापमान में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है
2. ग्लोबल वार्मिंग के नवीनतम प्रभाव
हाल के वर्षों में आए प्राकृतिक आपदाओं (जैसे 2023 में आई बाढ़ एवं जंगलो की आग) क ग्लोबल वार्मिंग के वर्तमान प्रभाव को दर्शाता है
गर्म हवाओं की वजह से गर्मी की लहरें (Heatwaves) और लंबी हो रही हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
3. विज्ञान और तकनीक का योगदान: जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक जैसे कार्बन कैप्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs), स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स एवं सोलर और विंड एनर्जी के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न नवीकरणीय ऊर्जा का भविष्य में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है।
4. समुदाय और व्यक्तिगत स्तर पर समाधान
व्यक्तिगत स्तर पर ऊर्जा की बचत, पेड़ों की देखभाल, सिंगल-यूज प्लास्टिक से बचना, और अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग।
सामाजिक जागरूकता अभियानों चलाये जाये , जैसे भारत में स्वच्छ भारत अभियान और हरित भारत मिशन।
5. प्रेरणादायक उद्धरण
कुछ प्रसिद्ध पर्यावरणविदों या नेताओं के कथन:
महात्मा गांधी का कथन: “पृथ्वी हर मनुष्य की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन हर मनुष्य के लालच को नहीं।”
अल गोर का कथन: “जलवायु परिवर्तन एक नैतिक संकट है, और इसे दूर करने के लिए दुनिया के प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।”
6. भविष्य की दिशा: क्या हो सकता है?
भविष्य में अगर ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित नहीं किया गया, तो इसमें ध्रुवीय बर्फ के पूर्ण पिघलने से समुद्र स्तर में वृद्धि और तटीय शहरों के डूबने का खतरा शामिल है।
7. नवीनतम समझौते और सम्मेलन
2023 में जलवायु सम्मेलन हाल में दुबई में हुए COP28 सम्मेलन, जिसमें देशों ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने की नई प्रतिबद्धताएँ दी हैं।
अगला cop सम्मेल्लन cop 29 अज़रबैजान में नवम्बर 2024 में होगा
8. संविधान में जलवायु और पर्यावरण के अधिकार का उल्लेख
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48A के तहत राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे और वनों और वन्यजीवों का संरक्षण करे।
ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े अंतरराष्ट्रीय और भारतीय संगठन
ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के संगठन कार्य कर रहे हैं। इन संगठनों का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नियंत्रित करना, और सतत विकास को बढ़ावा देना है। यहाँ कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और भारतीय संगठनों का विवरण दिया गया है:

अंतरराष्ट्रीय संगठन
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC): Global Warming in Hindi
स्थापना: 1992 में।
मुख्य उद्देश्य: जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर समन्वय करना। यह संगठन अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों का आयोजन करता है और इसके अंतर्गत ‘पेरिस समझौता’ जैसे महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं।
पेरिस समझौता (2015): यह एक ऐतिहासिक समझौता है, जिसमें देशों ने पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का संकल्प लिया। इसके तहत देश अपनी नीतियों में सुधार कर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC):
स्थापना: 1988 में, संयुक्त राष्ट्र और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा।
मुख्य उद्देश्य: जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक शोध करना और उसके प्रभावों की जानकारी देना। IPCC की रिपोर्ट्स जलवायु नीतियों को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। IPCC की रिपोर्टों से ही ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरों और संभावित समाधानों का पता चलता है।
ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF):
स्थापना: 2010 में UNFCCC के तहत।
मुख्य उद्देश्य: विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह संगठन स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं और जलवायु अनुकूलन कार्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।
क्योटो प्रोटोकॉल:
स्थापना: 1997 में।
मुख्य उद्देश्य: विकसित देशों द्वारा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने का लक्ष्य। हालाँकि यह प्रोटोकॉल 2020 में समाप्त हो गया, लेकिन इसने देशों को अपने उत्सर्जन को नियंत्रित करने की दिशा में जागरूक किया।
द वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF):
स्थापना: 1961 में।
मुख्य उद्देश्य: जैव विविधता की रक्षा करना और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने के लिए सतत परियोजनाओं को बढ़ावा देना। यह संगठन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने पर काम करता है।
क्लाइमेट रियलिटी प्रोजेक्ट:
स्थापना: 2006 में।
मुख्य उद्देश्य: ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जागरूकता फैलाना और राजनीतिक कार्रवाई को प्रेरित करना। इस संगठन के संस्थापक पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोर हैं।
भारत के संगठन
भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India – WII):
स्थापना: 1982 में।
मुख्य उद्देश्य: जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता पर हो रहे प्रभावों का अध्ययन करना। यह संस्थान वन्यजीव और पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करता है। Global Warming in Hindi
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD):
स्थापना: 1875 में।
मुख्य उद्देश्य: मौसम की जानकारी देना, जलवायु परिवर्तन की निगरानी करना, और प्राकृतिक आपदाओं के लिए पूर्वानुमान प्रदान करना। IMD का काम विशेष रूप से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों की निगरानी और पूर्वानुमान लगाने में महत्वपूर्ण है। Global Warming in Hindi
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal – NGT):
स्थापना: 2010 में।
मुख्य उद्देश्य: पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर न्यायिक कार्यवाही करना। NGT ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिनका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों को हल करना है।
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE): Global Warming in Hindi
स्थापना: 1980 में।
मुख्य उद्देश्य: पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर शोध और जागरूकता फैलाना। CSE पर्यावरणीय नीतियों पर काम करता है और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए सरकारों को सलाह देता है।
द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI):
स्थापना: 1974 में।
मुख्य उद्देश्य: सतत विकास, ऊर्जा दक्षता और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर काम करना। TERI ने कई ऊर्जा संरक्षण और जलवायु परिवर्तन परियोजनाएँ चलाई हैं और यह भारत के जलवायु नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इंडियन क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क (ICAN):
स्थापना: एक नागरिक संगठन।
मुख्य उद्देश्य: जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता फैलाना और नीति निर्माताओं को स्थायी नीतियों की ओर प्रेरित करना। यह संगठन आम जनता और सरकार के बीच एक पुल का काम करता है।
भारत की जलवायु नीति और पहलें
राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन (National Action Plan on Climate Change – NAPCC):
स्थापना: 2008 में।
मुख्य उद्देश्य: भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए विभिन्न मिशनों का कार्यान्वयन। इसमें 8 मिशन शामिल हैं, जैसे सौर ऊर्जा मिशन, ऊर्जा दक्षता मिशन, और वनीकरण मिशन।
इंटरनेशनल सोलर एलायंस (ISA):
स्थापना: 2015 में भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से।
मुख्य उद्देश्य: सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और इसका उपयोग करके ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। ISA का मुख्यालय भारत में स्थित है और इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा की ओर वैश्विक स्तर पर अग्रसर करना है।
नेशनल एफलुएंट सिस्टम (National Clean Energy Fund – NCEF):
स्थापना: 2010 में।
मुख्य उद्देश्य: ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण करना।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग और सूचकांक
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स (CCPI):
प्रकाशन: जर्मनवॉच (Germanwatch) और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा।
2023 रैंकिंग: भारत को 8वीं रैंक मिली थी, जो इसे बेहतर जलवायु प्रदर्शन वाले देशों में से एक बनाता है।
CCPI का उद्देश्य: यह सूचकांक 63 देशों का आकलन करता है जो मिलकर विश्व के 90% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें चार प्रमुख घटक होते हैं: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग, और जलवायु नीति।
ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन:
2022 के आंकड़े: चीन सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश है, जो वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 30% हिस्सा है। अमेरिका दूसरे स्थान पर है (13%), और भारत तीसरे स्थान पर (7%) है।
भारत: 2022 में भारत का कुल CO2 उत्सर्जन 2.88 बिलियन मीट्रिक टन था।
एनवायरनमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स (EPI):
प्रकाशन: येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा।
2022 रैंकिंग: भारत 180 देशों में से 180वें स्थान पर था। यह रैंकिंग इस बात पर आधारित है कि कोई देश पर्यावरण के क्षेत्र में क्या सुधार कर रहा है, जैसे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, और संसाधनों का संरक्षण।
EPI स्कोर: भारत का स्कोर 18.9/100 था, जो इसे सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में रखता है।
ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े आपदाओं के आंकड़े:
2021 के आँकड़े: वैश्विक स्तर पर लगभग 400 बिलियन डॉलर की क्षति प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई, जिसमें से अधिकांश आपदाएँ जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी थीं।
प्रभाव: जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली बाढ़, सूखा, और जंगल की आग जैसे आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ गई है।
पेरिस समझौते के तहत उत्सर्जन लक्ष्य:
भारत का लक्ष्य: भारत ने 2070 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने का वादा किया है। इसके तहत 2030 तक भारत अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 GW तक बढ़ाएगा और कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करेगा।
भारतीय सूचकांक और रैंकिंग
भारत की जलवायु परिवर्तन नीति रैंकिंग: Global Warming in Hindi
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा हाल ही में जलवायु से जुड़ी नीतियों को लागू करने में भारत ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, विशेषकर वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए।
राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा मिशन:
सोलर एनर्जी क्षमता: 2022 में, भारत ने सौर ऊर्जा में 50 GW से अधिक स्थापित क्षमता हासिल की, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में से एक बनाता है।
लक्ष्य: 2030 तक, भारत ने 450 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (GCRI):
प्रकाशन: जर्मनवॉच।
2023 में भारत: इस सूचकांक में, भारत सबसे अधिक जलवायु जोखिम वाले देशों में से एक रहा, जो लगातार बाढ़, चक्रवात, और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है। भारत 2023 में 7वें स्थान पर था।
क्लीन एनर्जी इंडेक्स:
भारत: स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। सरकार द्वारा 100 स्मार्ट सिटी परियोजना और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी योजनाओं ने स्वच्छ ऊर्जा के विकास में योगदान दिया है।
अन्य महत्वपूर्ण आँकड़े – Global Warming in Hindi
समुद्र स्तर में वृद्धि:
वैश्विक औसत समुद्र स्तर 1880 से अब तक लगभग 8-9 इंच बढ़ चुका है, जिसमें से लगभग एक-तिहाई वृद्धि पिछले 25 वर्षों में हुई है। भारत के कई तटीय शहर जैसे मुंबई, चेन्नई, और कोलकाता को इसका गंभीर खतरा है।
आर्कटिक में बर्फ की कमी:
1979 से अब तक आर्कटिक में समुद्री बर्फ की औसत मोटाई में लगभग 40% की कमी आ चुकी है। यह वैश्विक तापमान वृद्धि के सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है।
ग्लोबल तापमान वृद्धि:
2020 तक, औसत वैश्विक तापमान 1.2°C बढ़ चुका है, जो 19वीं शताब्दी के औसत तापमान से अधिक है। अगर इसी गति से तापमान बढ़ता रहा, तो यह 2050 तक 2°C से अधिक हो सकता है।
ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय और भारतीय रैंकिंग और आंकड़ों को टेबल के रूप में नीचे प्रस्तुत किया गया है:
| सूचकांक/आंकड़ा | रैंकिंग/आंकड़े | विवरण |
| क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स (CCPI) 2023 | भारत: 8वीं रैंक | यह सूचकांक 63 देशों का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, और जलवायु नीति के आधार पर मूल्यांकन करता है। |
| ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (2022) | भारत: 3rd (7%) | भारत वैश्विक CO2 उत्सर्जन में तीसरे स्थान पर है। 2022 में कुल 2.88 बिलियन मीट्रिक टन उत्सर्जन हुआ। |
| एनवायरनमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स (EPI) 2022 | भारत: 180वां स्थान | भारत का स्कोर 18.9/100 था, जो इसे सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में रखता है। |
| ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े आपदाएँ (2021) | वैश्विक आर्थिक क्षति: $400 बिलियन | जलवायु परिवर्तन से जुड़ी बाढ़, सूखा, और जंगल की आग ने वैश्विक स्तर पर बड़ी क्षति पहुँचाई। |
| पेरिस समझौता (2030) | भारत का लक्ष्य: 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा | भारत ने 2030 तक 1 बिलियन टन CO2 उत्सर्जन कम करने और 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। |
| ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (GCRI) 2023 | भारत: 7वां स्थान | जलवायु जोखिमों का सामना करने वाले देशों में भारत उच्च स्थान पर है, जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है। |
| राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा क्षमता (2022) | भारत: 50 GW सौर ऊर्जा | भारत ने 50 GW से अधिक सौर ऊर्जा स्थापित की है, जो इसे शीर्ष सौर ऊर्जा उत्पादकों में शामिल करता है। |
| समुद्र स्तर में वृद्धि (1880-2020) | 8-9 इंच | वैश्विक औसत समुद्र स्तर में 8-9 इंच की वृद्धि हुई है, जिससे तटीय क्षेत्रों में खतरा बढ़ा है। |
| आर्कटिक में बर्फ की कमी (1979-2020) | 40% | आर्कटिक में समुद्री बर्फ की औसत मोटाई में 40% की कमी आई है। |
| ग्लोबल तापमान वृद्धि (2020 तक) | 1.2°C | औसत वैश्विक तापमान 19वीं शताब्दी के औसत से 1.2°C अधिक हो चुका है। |
ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में टॉप 10 देशों की रैंकिंग उन देशों के कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन के आधार पर की जाती है। नीचे 2022 के आंकड़ों के अनुसार, उच्चतम CO2 उत्सर्जन करने वाले शीर्ष 10 देशों की तालिका दी गई है: Global Warming in Hindi Global Warming in Hindi
| रैंक | देश | CO2 उत्सर्जन (बिलियन मीट्रिक टन) | वैश्विक उत्सर्जन में हिस्सेदारी (%) |
| 1 | चीन (China) | 11.47 | 30% |
| 2 | संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | 5.01 | 13% |
| 3 | भारत (India) | 2.88 | 7% |
| 4 | रूस (Russia) | 1.71 | 4.5% |
| 5 | जापान (Japan) | 1.16 | 3.1% |
| 6 | जर्मनी (Germany) | 0.72 | 2.1% |
| 7 | ईरान (Iran) | 0.67 | 1.8% |
| 8 | सऊदी अरब (Saudi Arabia) | 0.61 | 1.6% |
| 9 | दक्षिण कोरिया (South Korea) | 0.59 | 1.5% |
| 10 | इंडोनेशिया (Indonesia) | 0.52 | 1.3% |
विश्लेषण: Global Warming in Hindi
चीन सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है, जो वैश्विक CO2 उत्सर्जन का लगभग 30% उत्सर्जित करता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जिसका 13% उत्सर्जन में हिस्सा है।
भारत तीसरे स्थान पर है, जो लगभग 7% वैश्विक CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है।
इस तालिका को निबंध में जोड़ने से आपको यह स्पष्ट रूप से दिखाने में मदद मिलेगी कि किस देश का ग्लोबल वार्मिंग में कितना योगदान है, और इसे कम करने के लिए किस स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए।
- Also Read :
- “ग्लोबल वार्मिंग के खतरों को समझने के लिए, Greenpeace पढ़ सकते हैं।”
- “पिछले कुछ सालों में की गई रिसर्च को आप Science Direct पर पढ़ सकते हैं।”
- “ग्लोबल वार्मिंग पर अधिक जानकारी के लिए, आप United Nations Climate Change पर पढ़ सकते हैं।
- How to Increase Car Mileage: Tested Tips for Better Fuel Efficiency | Knowledge Factor
निष्कर्ष
ग्लोबल वार्मिंग एक जटिल समस्या है, लेकिन इसके समाधान हमारे हाथों में हैं। यदि हम सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाएँ, तो इस संकट से निपटा जा सकता है। समय रहते कदम उठाना हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करेगा।
About Us
Knowledgefactor.in delivers fresh and compelling content that’s useful and informative for its readers. Knowledgefactor.in is a news and information site providing visitors with Breaking News ,Tech News, Mobiles, Laptops, Auto, Gadgets, Telecom, Facebook, Whatsapp, Android, Windows, Programming and many more.Our prior aim is to update latest Tech News in people about Computer Science and Information Technology and we constantly develop our group of experts to accomplish the mission. Apart from this, we are also deep in researching over topics of Computer Science and Information Technology with our great members and inter-group seminars, meets and activities are arranged with time to explore Technology.


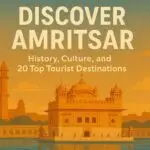

Helpful and great work.
thank you so much 🙂
Pingback: एक देश एक चुनाव क्या है ? (One Nation One Election in Hindi) फायदे , नुकसान, एवं जरूरत. | Knowledge Factor
Pingback: Flipkart Upcoming Sale 2025: All the Information About the Biggest Shopping Events of the Year | Knowledge Factor
An eye-opening reminder that global warming is real and urgent , we must act now to protect our planet for future generations.